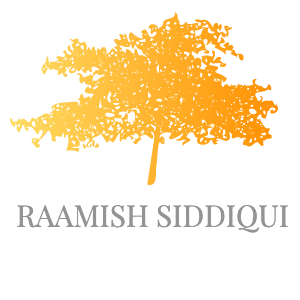क्यों कहते हैं मुहर्रम को शोक का महीना
इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है, जिसे मुहर्रम-उल-हराम के नाम से भी जानते हैं। यह इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक है। मुहर्रम पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की मृत्यु के शोक का महीना है। इस दिन शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं, जबकि सुन्नी ताजिया पुर्सी करते हैं। इस्लामिक विषयों के जानकार रामिश सिद्दीकी से जानते हैं कि मुहर्रम का इतिहास और महत्व क्या है?
मुहर्रम क्या है?
इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम साल का पहला महीना होता है। इस्लाम में साल के चार महीने मुहर्रम, रजब, ज़ुल-हिज्जा, ज़ुल-क़ादाह माह को बाकी महीनों पर श्रेष्ठता दी गई है। मुहर्रम का शाब्दिक अर्थ है मनाही, कुरान और हदीस के अनुसार, मुहर्रम के महीने में युद्ध या लड़ाई-झगड़ा करना निषिद्ध है। इस पवित्र महीने के समय मुसलमानों को अधिक से अधिक इबादत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस महीने की शुद्धता के कारण अनेकों लोग विश्वभर में इस महीने में रोजा यानी उपवास रखते हैं. इस्लामिक इतिहास के अनुसार, मुहर्रम के महीने में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं लेकिन उन सब में सबसे बड़ी और दुखद घटना थी हज़रत मुहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली और उनके परिवार का कर्बला के मैदान में निर्ममता से हुआ संहार।
मुहम्मद साहब के बाद कौन बनेगा खलीफा
हज़रत मुहम्मद साहब का निधन अरब के शहर मदीना में सातवीं शताब्दी में 632 ईसवीं में हुआ था। उनका निधन 63 वर्ष की आयु में हुआ था, निधन के बाद अरब समाज में शोक और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, शोक उनके चले जाने का और असमंजस स्थिति इसलिए क्योंकि वहां एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया था कि समाज का नेतृत्व अब कौन करेगा। उस समय मदीना शहर में उपस्थित सभी बड़े बुज़र्गों ने हजरत अबू बकर का चयन किया था, जो हजरत मुहम्मद साहब के सबसे करीबी साथियों में से थे। अबू बकर की मृत्यु के बाद हज़रत उमर इब्न खत्ताब को चुना गया, फिर उनकी मृत्यु के बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ्फान और उनके बाद हज़रत मुहम्मद साहब के दामाद हज़रत अली इब्न अबू तालिब को चुना गया। इन पहले चार चुने हुए लोगों के कार्यकाल को राशिदून खिलाफ़त कहा जाता है।
मुआविया के फैसले का लोगों ने किया विरोध
हज़रत अली के निधन के बाद दोबारा यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अगला ख़लीफा किसे चुना जाए। जहां कुछ लोग उनके बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन के समर्थन में आगे आए तो कुछ लोगों ने मुआविया का समर्थन किया। मुआविया मक्का के एक बड़े परिवार से थे और उस समय सीरिया के गवर्नर भी थे। इमाम हसन ने जब देखा के उनके दावेदारी से विवाद बढ़ सकता है तो उन्होंने मुआविया के साथ एक लिखित समझौता किया, जिसमें यह तय हुआ की मुआविया के बाद ख़िलाफ़त हज़रत हसन की तरफ लौट जाएगी और अगर इस बीच उन्हें कुछ हुआ तो उनके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन चुने जाएंगे। लेकिन मुआविया ने परंपरा और समझौते दोनों को तोड़ते हुए अपने अपने बेटे यज़ीद को अपनी जगह चुनने का फैसला किया। मुआविया के इस फैसले का वहां के कई वरिष्ठ लोगों ने विरोध किया, जिनमें हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला भी शामिल थे।

स्वयं को टकराव और नकारात्मकता के केंद्र से हटा लेना ही हज़रत इमाम हुसैन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है।
यज़ीद के सामने थी बड़ी चुनौती
यज़ीद के ख़लीफा बनते ही अरब की स्थिति बदल गयी। यज़ीद के बारे में इतिहास में आता है कि वे एक ज़ालिम शासक थे, जिनका झुकाव सिर्फ अपने हितों की तरफ था। यही कारण था कि लोग यज़ीद के ख़लीफा बनने के विरोध में थे। लेकिन यज़ीद के सामने बड़ी चुनौती हज़रत मुहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को अपनी तरफ मिलाने की थी क्योंकि वे हज़रत मुहम्मद साहब के नवासे थे और समस्त अरब समाज पर उनका काफी प्रभाव था।
यज़ीद ने उठाया सख्त कदम
यज़ीद ने कई बार अपने दूत के द्वारा इमाम हुसैन के पास पत्र भेजे कि वे यज़ीद की खिलाफत को मंजूरी दे दें, लेकिन वे इमाम हुसैन को अपनी तरफ लाने में सफल नहीं हो पाए। जहां एक तरफ यज़ीद अपने लोग भेज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ़ इमाम हुसैन के पास हज़ारों की तादाद में इराक में स्थित कूफा शहर के लोगों की तरफ से कूफा आने का न्योता भेजा जा रहा था, आखिरकार इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों के आमंत्रण पर परिवार सहित वहां जाने का फैसला किया. लेकिन यजीद को इमाम हुसैन का चुपचाप चले जाना भी मंज़ूर नहीं था। यज़ीद और उनके साथियों को डर था कि जिस तरह कूफा के लोग इमाम हुसैन को आमंत्रित कर रहे हैं अगर ऐसा ही हर शहर में होने लगा तो वे ज़्यादा दिन ख़लीफ़ा बन कर नहीं रह पाएंगे। इसलिए यज़ीद ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया ताकि कोई इमाम हुसैन का साथ देने की हिम्मत ना करे।
दूत की हत्या के बाद बना डर का माहौल
कूफ़ा पहुंचने से पहले इमाम हुसैन ने अपना एक दूत वहां भेजा, ताकि वहां के हालत का जायजा ले सकें, लेकिन दूत को यज़ीद की फ़ौज ने पकड़ लिया और उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। इसकी सूचना इमाम हुसैन को नहीं मिल पायी और वे कूफ़ा की तरफ़ निकल पड़े. दूत की हत्या के बाद कूफा के लोग इतना डर गए कि जब इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे तो कूफा का कोई व्यक्ति उनका साथ देने आगे नहीं बढ़ा, यहां तक कि कोई उनसे मिलने तक नहीं आया। जबकि उन्होंने ख़ुद हज़ारों की संख्या में पत्र भेजकर इमाम हुसैन को कूफ़ा आने का आग्रह किया था।
इस वजह से मुहर्रम में लगाते हैं पानी की सबील
इमाम हुसैन और उनके परिवार को कूफ़ा शहर के बाहर कर्बला के मैदान में यज़ीद की फ़ौज ने घेर लिया और उनका कहीं भी आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया। इमाम हुसैन वहां किसी युद्ध के इरादे से नहीं आए थे, इसलिए उनके पास ना हथियार थे और ना ही कोई फ़ौज। वे केवल अपने परिवार के साथ थे, जिसमें औरतें, बच्चे, भाई और बुज़ुर्ग थे। ये जानते हुए भी सत्ता में चूर यज़ीद के नुमाइंदों ने ऐसी बर्बरता दिखायी के नरसंहार से पहले उन्होंने इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों का पानी तक बंद कर दिया। यही कारण है कि दस मुहर्रम की तारीख़ के दिन अनेकों लोग जगह-जगह गरीबों के लिए पानी की सबील लगाते हैं और खाने का इंतज़ाम करते हैं। मुहर्रम की इस दसवीं तारीख को ‘आशूरा’ भी कहा जाता है।
इमाम हुसैन ने दिया सबसे बड़ा संदेश
इमाम हुसैन अगर चाहते तो यज़ीद की सत्ता से समझौता कर सकते थे। उन्हें केवल यज़ीद की ख़िलाफ़त को मंजूरी देनी थी, लेकिन ऐसा करने का मतलब होता कि वे एक ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर लेते जो हज़रत मुहम्मद साहब के बताए सच्चाई और इंसानियत के सिद्धांतों से बहुत दूर था। अगर इमाम हुसैन का उद्देश्य टकराव होता, तो वे अपने परिवार के साथ कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके कूफ़ा नहीं जाते, बल्कि मक्का में ही रहकर यज़ीद की सत्ता के विरोध में आवाज़ उठाते। स्वयं को टकराव और नकारात्मकता के केंद्र से हटा लेना ही हज़रत इमाम हुसैन के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है।
आज आशुरा के दिन को याद करते हुए हमें इमाम हुसैन के दिखाए इसी मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने टकराव के बजाय शांति के रास्ते को चुना। दरअसल यही मुहर्रम का संदेश है कि हम शांति और अमन की राह पर चलें।